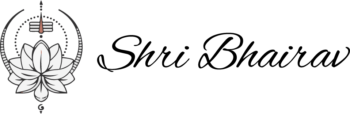झौंकता जाता था! और मंत्र पढ़े जाता था! "साधिके?" बोला मैं! वो खड़ी हो गयी, "नौदीये और प्रज्ज्वलित करो!" कहा मैंने, उसने नौ दीये लिए, कड़वा तेल डाला उनमे!
और फिर हाथों से बाती बनायी उनकी, और रख दी उन दीयों में! फिर मैंने अलख की अग्नि से उनको प्रवज्जलित कर लिया! "लो साधिके! दो दो दीये चारों दिशाओं में रख आओ!" बोला मैं,
और दीये उसके हाथों में रख दिए मैंने, दो दो करके, वो रखने लगी, और फिर रख आई! "ये एक दीया, मेरे सामने, वहाँ, दूर रख दो!" कहा मैंने! वो उठी और चल पड़ी सामने, और रख आई दीया! "आओ साधिके!" कहा मैंने,
अब उस साधिका की कोमल देह को रक्षित करना था, अन्यथा, कोई बाधा लग ही जाती! "यहाँ लेट जाओ!" कहा मैंने, वो लेट गयी, कमर के बल, अब उसके अंगों पर पुनः चिन्ह बनाये रक्त से, माथा, वक्ष, उदर, योनि, जंघाएँ, पिंडलियाँ और पाँव, "अब जो मैं बोलूंगा, दोहराना उसे" कहा मैंने, और अब उसे उल्टा लिटा दिया, पेट के बल, और फिर से उसकी देह पर चिन्ह बनाये, "खड़ी हो जाओ" बोला मैं,
खड़ी हो गयी,
"जाओ, वहां बैठी" कहा मैंने, बैठ गयी वहाँ वो,
और अब मैंने अपना श्रृंगार किया, मंत्र जपता जाता और श्रृंगार करता जाता!
और फिर दिया अलख में ईंधन! अलख उठी ऊपर!
और अब महाभीषण मंत्र पढ़े! और खड़ा हुआ! त्रिशूल उठाया अपना, एक चतुर्भुज बनाया भूमि पर,
और उस चतुर्भुज में एक ही अस्थि के ग्यारह टुकड़े रखे! "साधिके?" कहा मैंने, खड़ी हो गयी वो! "इधर आओ" कहा मैंने,
आ गयी वो, "इसमें जा बैठो बोला मैं, उसमे बैठ गयी! "सुनो साधिके?" बोला मैं, "अब चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं गिलं,या न गिळं, तुम्हे इस से बाहर नहीं आना है, समझी?" चेताया मैंने! उसने सर हिलाकर हाँ कही!
और फिर मैं जा बैठा अलख पर! और किया मंत्रोच्चार! सहसा ही हवा चली ज़ोरों से! दीयों की रौशनी भरभरा सी गयी! ज़मीन चाटने लगी थीं लौ उनकी
और फिर, पल भर में ही सब शांत! बस अलख की ही आवाज़! और कुछ नहीं! मेरे मंत्र फिर से आरम्भ हुए!
और तभी वातावरण में ताप बढ़ने लगा! पसीना छूटने लगा शरीर से! लेकिन श्रुति ठीक थी। वो ऐंद्राक घेरे में सुरक्षित थी! उसको पसीना नहीं आया था! मैंने देख लड़ाई!
और वहां! चीख रहा था बार बार नाम लेकर उन नौ के नौ का बार बार! "आदा!" "कुञ्चिका!" "त्रिहरना!" "भूषणा!" आदि आदि! वो भी अंतिम चरण में था और मैं भी! फिर खड़ा हुआ वो! रक्त का पात्र अपने सर पर उलट लिया उसने!
और फिर बैठ गया मंत्रोच्चार में! मैं भी यहां घोर मंत्रोच्चार में डूबा था!
और तभी मेरे यहां पर, छोटे छोटे सांप रेंगते दिखाई देने लगे! काले काले, छोटे छोटे सांप कोई उधर भाग रहा था, तो कोई उधर! फिर इकठ्ठा होते, फिर बिखर जाते!
और फिर लोप होते! ये चिन्ह था! रुरु का चिन्ह! रुरु बस, खोलने ही वाला था द्वार उनका! मैं एक बार फिर खड़ा हुआ! "श्रेष्ठ?" बोला मैं! उसने देखा एक नज़र! "अभी भी कुछ समय शेष है!" बोला मैं! थूका उसने!
"मान जा श्रेष्ठ!" बोला मैं! हंसा वो!
अपनी जांघ पर हाथ मारकर, हंसा वो! ये श्रेष्ठ नहीं हंस रहा था। ये उसका दम्भ हंस रहा था। अंत की ओर अग्रसर था उसका दम्भ!
और दम्भ का यही तो गंतव्य है! अंत!
और अंत भी ऐसा, कि पुनः कुछ आरम्भ ही न हो! प्रायश्चित भी न हो! ऐसा अंत! "श्रेष्ठ?" मैंने फिर से कहा! उसने फिर से धिक्कारा मुझे! मैं हंसने लगा! उसकी मूर्खता पर! "अपने पिता की सोच श्रेष्ठ?" कहा मैंने, नहीं बोला कुछ!
और ज़ोर से ईंधन झोंका उसने अलख में! "कुञ्चिका!" बोला वो!
आरम्भ हो गया था उसका आह्वान! और मैं नीचे बैठ गया! अलख के पास! सामग्री उठायी और, झोंक दी अलख में!
और अंतिम मंत्र, अब पढ़ने लगा मैं। बस कुछ देर और,
और उसके बाद, ये श्रेष्ठ, श्रेष्ठ नहीं रहने वाला था! आ जाना था यथार्थ में, जिसके लायक ही था वो श्रेष्ठ!
मैंने नेत्र बंद किये अपने! और समापन की ओर बढ़ चला! करीब दस मिनट बाद, मेरे नेत्र खुले, और तभी एक चटख लाल रंग का सा प्रकाश, हल्का सा प्रकाश उभरा वहां! श्रुति ने भी देखा उसे गौर से, वो चतर्भज में थी, इसीलिए देख पायी, अन्यथा नहीं देख पाती वो! वो लाल रंग का धुआं सा, पूरे स्थान पर फ़ैल गया था। अब तो निश्चित ही हो चला था कि उन नौ वीरों की सवारी बस आने को ही है। मैं अलख पर बैठा हुआ था, अलखनाथ का मंत्र पढ़ा
और झोंक दिया ईंधन! अलख लपलपाई ऊपर की तरफ! अब लड़ाई देख मैंने! और जो देखा तो अचम्भा हुआ! पूरा स्थान प्रकाश से कौंध रहा था! प्रकाश ही प्रकाश था वहां! ऐसा प्रकाश की आँखें चंधिया जाएँ! और उस प्रकाश में ही वो श्रेष्ठ, पढ़े जा रहा था मंत्र! और फिर वो खड़ा हुआ! भोग-थाल उठा लिया सर पर और जपने लगा मंत्र! बस, कुछ ही क्षणों में नव मातंग प्रकट होने ही वाली थीं! तडातड़ बिजलियाँ सी कौंध रही थीं, नीली नीली! आँखें फाड़, गले से तेज तेज पढ़े जा रहा था वो मंत्र! फिर उठा अलख से,और जा बैठा एक स्थान पर, भोग-थाल रखा, हाथ जोड़े, और चिल्लाने लगा! "प्रकट! मतंगा! प्रकट!" बार बार हाथों को नचाता! बैठता घुटनों पर, हाथ जोड़ता, और फिर से पढ़ने लगता मंत्र! और तभी धुंए का बवंडर सा उठा! और उस बवंडर में से, कुछ आकृतियाँ नज़र आने लगी! जैसे छाया! बड़ी बड़ी छाया! खड़ा हुआ वो! "मतंगा! मतंगा!" चिल्लाया वो! चिल्लाते चिल्लाते,
रोही पड़ा! "मतंगा! मतंगा! रक्षा! रक्षा!" रोते रोते बोला वो! इधर मेरे यहां प्रचंड वायु चलने लगी! सामग्री उड़ने लगी। दीये बुझने लगे। अलख ज़मीन को प्रणाम करने लगी! मेरे केश उड़ कर मेरे मुंह पर आ गए! मेरी मालाएं उड़ने लगी! मनके बजने लगे!
लेकिन श्रुति, श्रुति पर कोई असर नहीं! वो जस की तस बैठी थी! रुरु के आबंध में थी, इसीलिए। मैं भी संतुलन बनाये खड़ा रहा किसी तरह!
और अचानक ही सब शांत! धम्म धम्म की आवाजें आने लगी! जैसे ज़मीन पर बड़े बड़े घन गिर रहे हों आकाश से! ये क्या था! शायद लौह-दण्ड के प्रहार! या फिर दबाव! भूमि पर किसी शक्ति का दबाव! मैंने जिनका आह्वान किया था, वही प्रकट होने वाले थे! प्रत्यक्ष तो नहीं, अदृश्य रूप में ही! हाँ, वे हैं वहां, अब महसूस किया जा सकता था! वातावरण में गर्मी फ़ैल गयी थी बुरी तरह से, मेरी अलख की आंच ऐसी लग रही थी जैसे कोई चिता, जैसे मैं संग ही बैठा हूँ उसके!
और हुंकार उठी!
हंकार!
सीना फाइने वाली हुंकार! ऐसी हुंकार कि, प्रेत तो जा छिपें जहां जगह मिले उनको!
दूसरी शक्तियां सम्मुख ही न आएं। अब मैंने श्री रक्तज जी के मंत्र पढ़ने आरम्भ किया!
और अगले ही पल, बड़े बड़े पत्ते से हवा में बहने लगे! हवा फिर से चलने लगी थी! पत्ते भी ऐसे थे, जैसे काठगूलर के होते हैं। पत्ते भूमि पर गिरते और लोप हो जाते! अद्भुत सा नज़ारा था ये सब!
और तभी, बिजली सी कड़की! मित्रगण!
मुझे अट्टहास सुनाई पड़ा!
अट्टहास उस श्रेष्ठ का! हर दिशा से, हर दिशा से! शायद, नव-मातंग आ पहुंची थी वहाँ!
और अगले ही पल, प्रकाश फूटा! नौ पिंड दिखाई दिए! यही तो हैं नव-मातंग! लेकिन! लेकिन! वे पिंड, जस के तस वहीं स्थिर हो गए थे। मैं झुक गया था उस प्रकाश की चौंध से!
और अब खड़ा हुआ धीरे धीरे! और उस अद्भुत नज़ारे को देखने लगा था मैं! प्रकाश से प्रकाश कैसे कटता है, देख रहा था मैं! मैंने तो प्रकाश का प्रकाश को अंगीकार करना ही देखा था!
और हुई हुंकार! प्रबल हंकार! ऐसी हंकार, कि हाथी भी गश खा जाए उस हंकार से! जैसे स्वयं बादल फट पड़े हों ज़मीन पर! जैसे निर्वात फट पड़ा हो उस स्थान पर! वे नौ स्थिर पिंड, अभी भी वहीं थे! और फिर, अचानक से वो लाल प्रकाश पीले रंग का हो गया! घंटे से बजने लगे वहां! तुमुल स्वर से गूंजे शंखनाद के! चेकितान के से स्वर गूंज उठे। और फिर प्रकाश का जैस एको बड़ा सा गोल फटा! और देखते ही देखते, वो नौ पिंड क्षण में लोप हो गए!
और मैं!
हा! हा! हा! हा! मैंने अट्टहास किया!
और अट्टहास! नव-मातंग समाप्त! निकल गयी ये सिद्धि भी उसके हाथ से!
अब क्या बचा? मात्र दम्भ!
और शेष कुछ नहीं! कुछ नहीं! और अब! अब मैं भागा उस प्रकाश के नीचे!
और लेट गया। नेत्र बंद हो गए मेरे अपने आप! मेरे मुंह से, श्री रक्तज जी के ही मंत्र फूटते रहे! मैं जैसे अपन आप खो रहा था! प्रसन्न था और प्रसन्नता का मद मुझे समा गया था! मैं किसी तरह से खड़ा हुआ! हाथ जोड़ता हुआ! हाथ जोड़ता, आगे चला गया। ऊपर देखा! मेरा उद्देश्य पूर्ण हो चला था! अब और कुछ नहीं चाहता था मैं! कुछ नहीं! मैंने फिर से एक मंत्र पढ़ा, जिसमे गान था श्री रक्तज जी के आशीर्वाद का!
और फिर, वो प्रकाश लोप हुआ! आकाश में लहर सी खाकर "रुरु?" मैं चिल्लाया! "रुरु?" कहा मैंने!
और तभी मेरी लख भड़क उठी एकदम अपने आप! वहीं था रुरु और वे तीनों द्वारपाल!
मैं भागा पीछे अलख के पास!
और कपाल कटोरे में मदिरा परोसी! रुरु का एक मंत्र पढ़ा और गटक गया मैं वो मदिरा! अब बैठा अलख पर! ईंधन झोंका मैंने!
और मेरा चेहरा लाल हा अब! अब! अब दंड देना था उस श्रेष्ठ को! दण्ड भी ऐसा, जिसे मरते दम तक याद रखे वो! अंतिम सांस तक याद रहे उसको वो दंड! ऐसा दण्ड!
और दे दिया भोग अलख में! मैंने अलख में ईंधन झोंका! और खड़ा हुआ! त्रिशूल उठाया अपना, और एक चिन्ह बनाया मैंने भूमि पर, एक त्रिकोण और उसके साथ में एक छोटा त्रिकोण! उसमे कुछ लिखा ऊँगली से अपनी! और इसके बीचोंबीच कपाल कटोरे में मदिरा परोस कर, उस छोटे त्रिकोण के बीच में रख दी! उठा, और अलख पर पहुंचा! ईंधन झोंका, रक्त के छीटें डाले, और तब अपनी साध्वी को देखा, मुस्कुराते हुए! "आओ साधिके!" बोला मैं! वो निकल आई उस चतुर्भुज से! "बैठो यहां!" कहा मैंने, बैठ गयी! "ये लो! और दो भोग अलख में!" मैंने कुछ देते हुए कहा उसे! उसने दे दिया अलख में भोग! और अलख उठी ऊपर कोई चार फ़ीट!
अब लड़ाई देख! "श्रेष्ठ?" चीखा मैं! श्रेष्ठ, बैठा हुआ था। चुपचाप! सिहरता हुआ! सामने देखता हुआ! मुझे, दया सी आ गयी! न जाने क्यों! पता नहीं क्यों! मैं मुस्कुरा पड़ा, अलख में भोग नहीं डाला, रुरुका मंत्र भी नहीं पढ़ा! "श्रेष्ठ?" कहा मैंने,
उसने देखा सामने! "अभी भी समय है!" कहा मैंने! पत्थर सा बैठा था, बैठरहा! "मैंने मना किया था श्रेष्ठ। मना किया था। अब क्या रहा तू?" पूछा मैंने, रो पड़ा! बस बुक्का नहीं फाड़ा! आंसू निकल आये उसके! "क्षमा मांग ले श्रेष्ठ!" कहा मैंने! वो खड़ा हुआ! आंसू पोंछे! और अपना त्रिशूल उखाड़ लिया भूमि से! और हो गया तत्पर किसी से भी भिड़ने को। मन ही मन कुछ पढ़े, लेकिन शब्द बाहर न आएं गले से, मुंह से! नहीं माना वो। मैंने तभी अलख में भोग दिया!
और पढ़ डाला मंत्ररुरु का! और बता दिया उद्देश्य! रूर, हवा की गति से निकला वहां से! वायु वेग के संग!
और जा पहुंचा उधर! वायु ऐसी चली, कि खड़ा होना मुश्किल हो गया उस श्रेष्ठ का! चेहरे पर भय, शरीर में कम्पन्न! गिर पड़ा! फिर उठा! त्रिशूल उठाया!
और जैसे किसी ने उसको उसकी गर्दन से पकड़ कर फेंका पीछे! त्रिशूल छूटा हाथ से उसने! बहुत तेज खन्न की आवाज़ हुई!
पत्थर पड़े थे वहां! श्रेष्ठ फिर से फिका हवा में, और जा गिरा कोई पचास फ़ीट आगे! मुंह से आह या कोई कराह भी न निकली!
अगले ही पल, उसका एक हाथ उखड़ा, हवा में फेंक दिया गया! मांस के लोथड़े बिखर गए वहाँ!
रक्त ही रक्त!
और तब चीख निकली थी श्रेष्ठ की! फिर से हवा में उछला,
और गिरा नीचे! घसीट लिया किसी ने उसको! हवा में उठा और एक टांग घुटने से तोड़ डाली, फेंक दी अन्धकार में!
खूनमखान हो गया था श्रेष्ठ! "क्षेवांद! क्षेवांद रुरु! क्षेवांद!" कहा मैंने!
मांस के पिंड सा, एक बड़े से पिंड सा पड़ा हुआ था श्रेष्ठ वहां!
और अगले ही पल, उसके केशों में आग सुलग उठी! हो गया खाली,सदा सदा के लिया! पात्र टूट गया! सब खत्म! सब खत्म!
और रुरु वापिस! मैंने अल्वेक्षण मंत्र पढ़ा!
नौ बार! एक एक वीर का धन्यवाद किया!
और प्रणाम किया! तत्क्षण ही, वायुवेग बंद हो चला! रुरु चला गया था वापिस! अपने तीनों ही द्वारपालों के संग! मैं भागा पीछे! अपनी साध्वी से जा लिपटा! "हम विजयी हुए! हम विजयी हुए!" लिपटे लिपटे कहा मैंने! उसने भरा मुझे बाजुओं में, और मेरा चेतना अब लोप होने लगी!
आँखें बंद होने लगी, और मैं अचेत हो गया! फिर क्या हुआ, कुछ नहीं पता! कुछ भी नहीं! सुबह जब में आँख खुली, तो मुझे सुबह ही लगी वो! लेकिन तब तक चार बज चुके थे!
सभी बैठे थे वहाँ! शर्मा जी, चिंतित से! बाबा मैहर, चंदा और वो श्रुति, मेरे पांवों के पास बैठी थी! मैं मुस्कुरा पड़ा शर्मा जी को देखकर! वो उठे,और आ गए मेरे पास! मैं बैठ चुका था तब तक मुझे गले से लगा लिया! बाबा मैहर ने भी गले से लगाया! मित्रगण!
सरभन आठ दिन जिया और उसके बाद उसके जीवन ने प्रपंच किया उसके साथ ही उसको हृदयघात हुआ, और मृत्यु हो गयी उसकी! श्रेष्ठ, एक भुजा, और एक टांग गंवा बैठा था, उसकी एक आँख भी चली गयी थी, वर्ष २०१३ की सर्दियों में, उसकी भी मृत्यु हो गयी! मैं बाबा धर्मेक्ष से और उस युक्ता से कभी नहीं मिला फिर! आज तक नहीं! हाँ, न मुझ तक बाबा धर्मेक्ष की कोई खबर ही आई आज तक!
हाँ! श्रुति में संग ही रही! दो महीने तक, संग ले आया था उसे! आज भी संग ही है मेरे, सशरीर भले ही न हो, लेकिन मेरे मन में! सदा ही रहेगी! मित्रगण! दम्भ खोखला होता है, बुलबुला, पानी का बुलबुला! ताव तो बहुत देता है, लेकिन घाव भी बहुत देता है! घाव ऐसा, जो रिसता ही रहता है! कभी नहीं भरता! हाँ, एक बात और, मुझे उस सरभंग का कोई अफ़सोस नहीं, लेकिन उस श्रेष्ठ का है, तिल का ताड़ बना दिया था उसने! क्या मिला? कुछ नहीं! इसीलिए, दम्भ जब भी चढ़े, तो खुद को छलनी कर लो विवेक की तलवार से!
----------------------------साधुवाद!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------