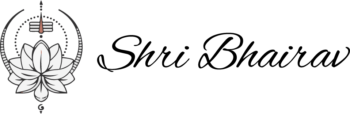इस रखवाले का मिला, तय है! ये अवश्य ही मिलेगा, सभी को! ये उपवन भी मिलेगा, सभी गुजरेंगे इस उपवन से! ये मार्ग सभी को पार करना होगा! यहां की सुंदरता देख, सब कुछ भूल जाएंगे हम लोग, ऐसा महसूस होता है! ऊँचे ऊँचे पेड़, घने, छायादार, फलों से लदे हुए, फलों की सुगंध पवन में घुली होगी! परन्तु, इस सुगंध को, मात्र वही सूंघ सकेगा, जिसने उस पर पार पायी हो! अर्थात, एक ऐसी अवस्था, कि, आप सिर्फ वही सूँघों जो आप सूंघना चाहते हों! कैसा अच्छा हो, की दुर्गन्ध, पलट कर एक सुगंध बन, नथुनों में लौटे! क्या ही अच्छा हो! खैर, ये साधन है, साधन करना होता है, तभी कुछ हाथ लगता है! बिन हाथ हिलाये तो, देह भी नहीं खुजाई जा सकती! अब चूँकि, ये संस्मरण अपने अंतिम चरण की अंतिम पंक्ति में है, तो मैं अब घटना से संबंधित वर्णन करना ही उचित समझूंगा!
"साधिके?" पूछा मैंने,
"नाथ!" बोली वो, आनंदमय सी!
"आनंद में हो साधिके?" कहा मैंने,
"परम-आनंद समान मेरे नाथ!" बोली वो,
परम-आनंद! बहुत ही गूढ़ सा अर्थ है इसका! हंसना, ठहाके मार, लोट-पोट होना, हंसी रोके न रुके, या उदर में पीड़ा हो, ये आनंद, आनंद नहीं! ये तो कुछ भी नहीं! जिस आनंद में, गूढ़-गम्भीरता हो, वही इस परम-आनंद का द्वार है! इस परम-आनंद को, न किसी के व्यंग्य की, न किसी की व्यंग्यात्मक-दशा की, न फूहड़ता की कोई आवश्यकता ही नहीं! न किसी के संग की, न किसी के मिलन की, न किसी की प्रतीक्षा ही, न किसी का बिछोह हो, उसका दुःख, न कोई जन्मा हो, उसका सुख, कोई आवश्यकता ही नहीं! ये हे परम-आनंद! तो मेरी साधिका ने, गूढ़ उत्तर दिया था की वो, उस समय, परम-आनंद की स्थिति में पहुंच चुकी थी! मित्रगण! इस परम-आनंद को प्राप्त करने के लिए, करवाने के लिए, न जाने कितने धर्म-गुरु, धर्माचार्य, धर्मोपदेशक, आये और गए! आते रहेंगे और जाते भी रहेंगे! कोई थाह न पाया इसकी! वो, परम-मार्ग ही न मिला किसी को! किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ, किसी ने कुछ बताया और किसी ने कुछ! अंतर कुछ नहीं! बस, शब्दों के फेर का ही है! मेरे यहां गमला कुछ अलग तरह से बनता है, तेरे यहां कुछ और तरह से! लेकिन रोपा तो पौधा ही जाता है दोनों में! तेरे यहां थाल चौकोर है, मेरे यहां गोल, भोजन दोनों में ही होता है! बस, यही फेर है! मेरे यहां शव, अग्नि में दाह किया जाता है, तेरे यहां दफन! होना दोनों को ही मिट्टी है! बस, यही, कुछ अंतर है, नहीं तो चाँद भी वही, सूरज भी वही, पानी भी वही, हवा भी वही! ज़मीन मेरी भी वही, तेरी भी वही! तो इस परम-आनंद को, सभी ने, अपने अपने हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से, समझाया है! अब कोई कितना सत्य है, ये बताने वाला तो कोई और ही है! और वो जो है, वो सदैव चुप ही रहता है! बस देखता है, मोहरे बदलता है और फिर से चुप हो जाता है! अब कोई काले पे खड़ा होता है तो कोई सफेद पर! ये उसकी रजा! उसकी इच्छा! खैर साहब! इस विषय का न कोई अंत और न ही कोई ठहराव! तो, छोड़ना ही बेहतर! छोड़ देते हैं!
"नाथ?" बोली वो,
"हाँ साधिके?'' बोला मैं,
"कुआं!" बोली वो,
"अच्छा!" कहा मैंने,
"हाँ नाथ!" बोली वो,
"समीप हो इसके?" पूछा मैंने,
"हाँ नाथ!" बोली वो,
"कैसा है?" पूछा मैंने,
"बहुत ही बड़ा!" बोली वो,
"जल-निकासी कैसे होय?" पूछा मैंने,
"सीढ़ियां हैं नाथ!" बोली वो,
"झांको इसमें!" कहा मैंने,
"आदेश नाथ!" बोली वो,
"चढ़ो सीढ़ियां!" कहा मैंने,
"हाँ नाथ!" बोली वो,
"हाँ साधिके!" कहा मैंने,
"नाथ???" बोली वो,
"क्या हुआ?" पूछा मैंने,
"अंदर तो जैसे रक्त है?" बोली वो,
"हाँ! रक्त ही है!" कहा मैंने,
"तो ये उपवन...?" बोली वो,
"रक्त से सींचा जाता है!" कहा मैंने,
"किसका रक्त?" पूछा उसने,
"स्वतः ही आता है इस कुँए में!" कहा मैंने,
"तब ये रक्त नहीं नाथ!" बोली वो,
"अब समझीं तुम!" कहा मैंने,
"मैं समझ गई! नाथ!" बोली वो,
"आओ, उतरो अब!" कहा मैंने,
"आदेश नाथ!" बोली वो,
"हाँ, उतर आओ!" कहा मैंने,
"नाथ?? नाथ?" बोली वो,
"हाँ साधिके?" पूछा मैंने,
"कुछ दिखा मुझे!" बोली वो,
"क्या?" पूछा मैंने,
"कोई है, हल थामे हुए!" बोली वो,
"वही है रखवाला!" कहा मैंने,
"अच्छा!" बोली वो,
"जाओ, मार्ग पूछो!" कहा मैंने,
"हाँ नाथ!" बोली वो,
और फिर से शांत हो गई वो! लेकिन चेहरे पर, संतोष के भाव उभरते जा रहे थे, बार बार! मेरी साधिका, विचरण जो कर रही थी, उस पार का!
"हाँ साधिके?" कहा मैंने,
"मार्ग बता दिया उन्होंने!" बोली वो,
"क्या साधिके?'' पूछा मैंने,
"बाएं चलने पर, एक कन्दरा है, बड़ी, उसमे ही जाना है!" बोली वो,
"अंतिम स्थल!" कहा मैंने,
"तो चलो उधर साधिके!" कहा मैंने,
"हाँ नाथ!" बोली वो,
और एक झटका सा खाया उसने!
"क्या हुआ साधिके?" पूछा मैंने,
"मैं रुक गई हूँ नाथ!" बोली वो,
"क्यों? क्या कारण है?" पूछा मैंने,
"ये अंतिम-स्थल है?" पूछा उसने,
"हाँ साधिके!" कहा मैंने,
"ओह नाथ...मेरे दुर्भाग्य!" बोली वो,
"दुर्भाग्य? साधिके?" पूछा मैंने,
"मैं नहीं लौटना चाहती यहां से नाथ!" बोली वो,
"वचन-भंग नहीं करना साधिके!" कहा मैंने,
"हे साधक?" बोली वो,
मैं चौंक पड़ा! साधक? उसने ऐसा कहा?
"साधिका?" कहा मैंने,
"क्षमा! क्षमा!" बोली वो!
"साधिके! अब देर नहीं!" कहा मैंने,
उस पर, अब वेग चढ़ने लगा था, ये वेग कहीं, कुछ अहित न करा दे, अब मुझे तेजी से कार्य संचालित करना था! यहां आकर, उसका सूक्ष्म यदि रुक जाता तो निःसन्देह, वो मृत ही ढुलक कर गिर पड़ती मेरे ऊपर से! वो, क्रिया-प्रभाव में थी, क्रिया के सहारे ही, वो उस पार का गमन, निरंतर किये जा रही थी! मेरे शब्दों के सिवाय, उसे और कुछ सुनाई नहीं पड़ना चाहिए थे, यदि उसने ध्यान लगाया कहीं और, तो समझो, श्वास पूर्ण हुईं उसकी!
"साधिके?" मैंने स्नेह रूपी बाहव से पूछा!
"नाथ!" बोली वो,
"कन्दरा दीख पड़ी?" पूछा मैंने,
"नहीं नाथ!" बोली वो,
"क्या देखती हो?" पूछा मैंने,
"पुष्प ही पुष्प! ये किसने रोपे हैं? ये कतारें, कैसे बनी हैं? ये पीले फूल, एक कतार में हैं, फिर लाल, और फिर एक संकरा सा मार्ग, और फिर से नीले पुष्प! नाथ, यहां के सभी वृक्ष फूलों से लड़े हुए हैं! नाथ, जी नहीं चाहता यहां से डिगने को! मेरी मदद करो नाथ! मुझे रोक दो नाथ! आप कर सकते हो नाथ! रोक दो! मैं नहीं लौटना चाहती मेरे नाथ! मुझे रोक दो यहीं! रोक दो! रोक दो!" स्वर, पहले ऊँचे थे, फिर मद्धम हुए, और फिर, धीरे धीरे, उसके गले में, रुन्धते चले गए!
"असम्भव!" कहा मैंने,
"स्वीकार कीजिये नाथ!" बोली वो,
"असम्भव!" कहा मैंने,
"आप, सम्भव बना सकते हैं! दया कीजिये!" बोली वो,
"नहीं, मेरे हाथ, कुछ नहीं, आगे बढ़ो साधिके, रुकना नहीं है, आगे बढ़ो!" कहा मैंने,
"नाथ?" बोली वो,
"नहीं साधिके!" कहा मैंने,
"नाथ, तनिक विचारिये, नाथ?" बोली वो,
"साधिके?" मैं बोला गुस्से से तब!
"नाथ?" बोली वो,
"आगे बढ़ो!" बोली वो,
"मैं थक चुकी हूँ!" बोली वो,
"मिथ्याभाषी! साधिके? आगे बढ़ो? ये मेरा आदेश है!" कहा मैंने,
"नाथ?" बोलते बोलते, रो पड़ी वो!
"साधिके?" कहा मैंने,
"नाथ?" बोली सुबकते हुए!
"आगे बढ़ो!" कहा मैंने,
"अवश्य नाथ!" बोली वो,
और चल पड़ी फिर से आगे, समझाया था मैंने, आन लगी थी, वचन की, बढ़ना पड़ेगा, सो बढ़ गई आगे!
"ओ मेरे नाथ! विहंगम!" बोली वो,
"क्या हुआ?" पूछा मैंने,
"अनुपम सौंदर्य!" बोली वो,
"क्या देखती हो?" पूछा मैंने,
"जल-धाराएं!" बोली वो,
"ओह! अच्छा!" कहा मैंने,
"मैं पास खड़ी हूँ एक धारा के नाथ!" बोली वो,
"और?" पूछा मैंने,
"श्वेत जल है!" बोली वो,
"और?" पूछा मैंने,
"नीली सी मछलियां हैं इसमें नाथ!" बोली वो,
"और?" पूछा मैंने,
"जल शांत है!" बोली वो,
"बाएं देखो!" कहा मैंने,
"हाँ नाथ!" बोली वो,
"जाओ उधर!" कहा मैंने,
"आदेश नाथ!" बोली वो,
और वो, चल पड़ी!
"पहुंच गई!" बोली वो,
"धारा, संकरी हुई?" पूछा मैंने,
"हाँ नाथ!" बोली वो,
"इस लांघ लो!" कहा मैंने,
"हाँ नाथ!" बोली वो,
"अब फिर से बाएं देखो!" कहा मैंने,
"हाँ........................." बोली और रुकी!
"कन्दरा! जाओ!" कहा मैंने,
"आदेश, नाथ! मैं जाती हूँ!" बोली वो,
और फिर से, शांत हो गई, शांतचित्त सी, आगे बढ़ती रही वो, अब, ये सम्पूर्ण क्रिया, बस, कुछ ही शेष थी!
"साधिके?" कहा मैंने,
"नाथ?" बोली वो,
"अब कोई प्रश्न नहीं!" कहा मैंने,
"जी नाथ!" बोली वो,
"तुम, अब वैसा ही करना, जैसा मैं तुमसे कहता हूँ!" कहा मैंने,
"आदेश नाथ!" बोली वो,
"कन्दरा, कितनी दूर?" पूछा मैंने,
"कुछ ही दूर!" बोली वो,
"साधिके!" कहा मैंने,
"नाथ?" बोली वो,
"क्या कोई मार्ग दीखता है, कन्दरा तक ले जाने के लिए, तुम्हें?" पूछा मैंने,
"हाँ नाथ!" बोली वो,
"कहाँ है वो मार्ग?" पूछा मैंने,
"मेरे समक्ष!" बोली वो,
"तो जाओ!" कहा मैंने,
"नाथ!" बोली वो,
"मैं चल रही हूँ नाथ!" बोली वो,
"हाँ, चलती रहो!" कहा मैंने,
"बस, कुछ ही दूर, नाथ!" बोली वो,
"ठीक!" कहा मैंने,
"नाथ? नाथ?" बोली वो,
"क्या हुआ साधिके?" पूछा मैंने,
"नाथ? यहां, मार्ग नहीं है, नीचे के लिए, सीढ़ियां हैं, द्वार बहुत बड़ा हैं, मुझे, शीर्ष नहीं दीख रहा?" बोली वो,
"मत घबराओ! आगे बढ़ो!" कहा मैंने,
"हाँ नाथ!" बोली वो,
और फिर से शांत हुई!
"नाथ?" बोली वो,
"बोलो साधिके?" पूछा मैंने,
"नाथ, ये कैसी घोर माया है?" पूछा उसने,
"माया? कैसी माया?" पूछा मैंने,
"नाथ, यहां, कपाट नहीं हैं, चौखट है परन्तु, न आरम्भ ही दीखता है और न अंत ही?" बोली वो,
"समझ रहा हूँ, तुम सीढ़ियों पर ध्यान केंद्रित करो बस!" कहा मैंने,
"आदेश नाथ!" बोली वो,
कुछ पल, शांत! कुछ पल, फिर ज़ोर ज़ोर से कांपने लगी वो!
"साधिके?'' पूछा मैंने,
कोई उत्तर नहीं दिया उसने!
"साधिके? कहाँ हो?" पूछा मैंने,
"न...न......नाथ? नाथ?" बोली वो,
"क्या हुआ? क्या हुआ?" पूछा मैंने,
उसका सर, पीछे ढुलक गया था, मैंने उसको, उसकी भुजाओं से थाम रखा था! नहीं तो, मेरी जंघाओं के बीच से वो, नीचे गिर जाती!
"साधिके?" कहा मैंने,
"ना....थ....." बोली वो, जैसे, मद्य का सेवन किया हो उसने!
"साधिके?" चीखा मैं,
कोई उत्तर नहीं!
"साधिके? साधिके? साधिके?" कहा मैंने,
और तब मैंने एक मंत्र पढ़ा, पढ़ते ही, एक हाथ से उसको थामा और दूसरे हाथ से, मिट्टी की एक चुटकी उठा, उसकी नाभि पर रगड़ दी! उसी खांसी सी उठी, उसके होश क़ाबिज़ हुए! कुछ जान सी पड़ी उसकी देह में!
"नाथ?" बोली वो,
"हाँ साधिके?" बोला मैं,
"यहां, अन्धकार है, गहन!" बोली वो,
"पीछे देखो?" कहा मैंने,
"रात्रि-समय है!" बोली वो,
"पीछे, दृश्य बदल गया है?" पूछा मैंने,
"हाँ नाथ!" बोली वो,
"ब्रह्म-वेला समाप्ति की ओर है साधिके, अब और विलम्ब नहीं!" बोला मैं,
"आदेश करें!" बोली वो,
"वहीँ रुको!" कहा मैंने,
और मैंने कुछ मंत्र, जल्दी जल्दी पढ़े!
"नाथ?" बोली वो,
"हाँ साधिके?" बोली वो,
"मेरा हाथ थाम लिया है किसी ने, लेकिन मैं, देख नहीं पा रही, कौन है वो नाथ? नाथ? मैं चेतना खो दूंगी, किसी भी क्षण, नाथ...क्षमा!" बोली वो,
और, उसने चेतना खो दी! उस भवन के, गहन अन्धकार में, जहां, कोई भी चेतना खो सकता है, खो दी अपनी चेतना! मैंने कोई प्रयास नहीं किया, जानता था, कोई लाभ नहीं! इस यात्र का अंत, मेरी साधिका के लिए, हो चुका था! परन्तु, मेरे लिए नहीं! हाँ! मेरे लिए नहीं!
मैंने अपने नेत्र बंद किये, कुछ स्मरण किया और फिर से नेत्र खोल दिए! साधिका को, पीछे, जंघाओं के बीच में से, आहिस्ता से पीछे छोड़ दिया! उसका सर अब, उस घाड़ के घुटनों के मध्य था, रखा हुआ, उसकी ढलान में, व्यवस्थित!
मैंने अब, डोर थामी! अब मुझे, अपने मंत्र-बल से, उस गहन अन्धकार को बींधना था! मैंने, गुरु-नमन किया! गुरु-आशीष मिले, अनुनय किया! आकाश को देखा एक बार और उस अघोर-पुरुष का स्मरण किया, जिसके कारण ही मैं, उस गहन अन्धकार में अब, प्रकाश ढूंढने, उतरने लगा था!
"माँ! आशीष दे माँ!" कहा मैंने मन ही मन!
"हे शक्ति-सम्वर्धनि माँ! आशीष दे!" कहा मैंने,
"हे मेरे भैरव नाथ! है मेरे भैरव नाथ! अब सब, तुझे समर्पित!" कहा मैंने,
एक महानाद! जय श्री भैरव नाथ!
मेरी साधिका ने चेतना खो दी थी! अब , वो चाह कर भी कुछ न कर सकती थी! मैं चाहता तो था कि वो मेरे साथ ही रहे! साथ ही, उस साधना का फल भी देखे! लेकिन, मनुष्य की अपनी ही कुछ सीमाएं हैं! वो दक्ष तो थी, लेकिन इतनी भी नहीं! आखिर में, ऊर्जा-स्राव और ऊर्जा-क्षय के कारण, अब चेतना-शून्य हो गई थी! उसमे, मुझे ऊर्जा-संचार करना था, और इतना समय मेरे पास था नहीं, मुझे अब किसी भी प्रकार से, उस गहन अन्धकार में, प्रकाश ढूँढना था, प्रकाश, उस दिव्यता का, जो, प्रस्फुटित हुआ करता है, मुझे यही ढूँढना था! तो मैं अब तत्पर हो गया था! ये अंतिम चरण था, कोई चूक नहीं चाहिए थी, कोई गुंजाइश भी न थी! तब मैंने, आगे बढ़ने का निश्चय किया! मैंने, 'प्रवेश' हेतु मंत्र पढ़ने आरंभ किया, ये मंत्र गूँज उठे! और किस पल, मैं उस गहन अन्धकार में प्रवेश कर गया, मुझे नहीं पता चला!
क्या मेरे नेत्र खुले हैं? मैंने, पलकें पीटीं अपनी! हाँ, मैं उसी गहन अन्धकार में हूँ! मेरे अंतःकरण से स्वर गूंजा ये! क्या मेरी साधिका, यहीं है? हाँ, यहीं है! फिर से स्वर गूंजा! मेरे लिए, क्या उचित है? साधिका को ढूँढना या फिर आगे बढ़ना? आगे बढ़ना! ये स्वर गूंजा! और ये निश्चित हो गया कि मुझे आगे ही बढ़ना है! मैं आगे बढ़ा! मेरे पांवों में, शीतल सा जल जैसे टकरा रहा था! मैं आगे बढ़ता जा रहा था, अँधेरे के भी दो पक्ष हुआ करते हैं, एक सघन और एक असघन! सघन, प्रकाश के सूक्ष्म से सूक्ष्म कण को भी परावर्तित नहीं करता, असघन में, प्रकाश सेंध लगा देता है! सेंध लगाते वक़्त, प्रकाश अपना, कुछ अंश, वहीँ छोड़ देता है, इस से पहले कि ये असघन, सघन में परिवर्तित हो, प्रकाश के कणों की आमद-जामद लगी रहती है! एक के अवशोषित होते ही, पुनः, दूसरा उसका स्थान ले लिया करता है! तो मैंने अपने आप को स्थिर खड़ा किया! और उस अंधकार के असघन-भाग को ढूंढा! कुछ अधिक ही परिश्रम सा हुआ, और मुझे बाईं तरफ, कुछ इसका पता चला, मैं उधर ही चल पड़ा! तत्व, चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म, कभी नियम भंग नहीं करते! स्थूल, गुरुत्व का आदर करता है और सूक्ष्म, परिधि का, परिधि किसकी, समय की, समय की भी एक सीमा होती है, कैसी सीमा भला? समय, सभी स्थानों पर, सदैव समान नहीं होता, इसका मान, निरंतर घटता और बढ़ता रहता है! वायुवृत में भी समयमान बदल जाता है! समय के नियम स्थिर हो सकते हैं, परन्तु, समय स्वयं ही समान नहीं रहता! ब्रह्माण्ड में, समय समान नहीं, ये देखा भी गया है! तो मेरा सूक्ष्म भी, उस समय, इन्हीं बन्धनों में बंध आगे बढ़ता जा रहा था! तीन इन्द्रियां मौखिक हैं, जो भान से जुडी हैं! पहली नेत्र, द्वितीय घ्राण, तृतीय रस, ये, सूक्ष्म में भी तभी कार्य करेंगी, जब आपका इन पर, पूर्ण अधिकार हो! अधिकार? इंद्रियों पर अधिकार? कैसे सम्भव? मित्रगण! असम्भव शब्द, खोखली जिव्हा, खोखले आत्म और खोखले ज्ञान का परिचायक है! कोई कार्य दुःसाध्य अवश्य ही हो सकता है, परन्तु असम्भव कदापि नहीं! तो फिर, किया क्या जाए? कोई सिद्धि? क्या सिद्धि इसके लिए आवश्यक है? हाँ है! बिलकुल आवश्यक है! परन्तु उस से भी आवश्यक है, सर्वप्रथम, स्वयं-सिद्ध होना! स्वयं-सिद्ध? इसका अर्थ? फिलहाल ये मेरा विषय नहीं यहां, हाँ इतना अवश्य ही, कि स्वयं-सिद्ध हुए बिना, कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती! मन आपका सिल है और इंद्रियां आपकी बट्टा! इनके बीच, समस्त संसार पिसे जा रहा है! पीसा जा रहा है, हम जानते भी हैं परन्तु, अनभिज्ञ बने रहते हैं! किसी दोष से मुंह फेरना हो, तो अनभिज्ञ बन जाओ! है न यही! नहीं करते हम सभी ये? या कभी किया नहीं? नहीं किया, तो नौबत कभी न लाना ऐसी मेरे मित्र! और जो हो गया हो, तो पुनः न हो, इसका ध्यान अवश्य ही रखना! ग्लानि किसे होती है? किसे? ज़रा सोचिये तो? उत्तर बेहद ही चौंकाने वाला होगा! जीवन का मूल-उद्देश्य क्या है? वही! ठीक वही, जो, इस सिल-बट्टे के बीच पिसे जा रहा है, पिसे जा रहा है! अब प्रश्न ये, कि ठीक है, मान लिया, पिसे जा रहा है! पिसे ही जा रहा है, लेकिन पीस कौन रहा है आखिर? कौन है वो? क्या ईश्वर? ईश्वर पीस रहा है? उत्तर है, नहीं! नहीं? तो कौन फिर? उत्तर है, हमारी अयोग्यता! असमर्थता नहीं! कोई असमर्थ है ही नहीं!
चलिए, आगे बढ़ते हैं!
हाँ, तो मैं उस असघन अन्धकार में प्रवेश करता गया, करता गया, लगा, युग ही न बीत जाएँ कहीं! कहीं यहीं न भटक जाऊं! कहीं, कभी प्रकाश देखूं भी या नहीं!
"रक्षाम!" निकला मुख से मेरे!
"रक्षाम!" फिर से कहा,
लेकिन ये क्या? मेरे तो शब्द, मुझे ही न सुनाई पड़े?
"रक्षाम!" मैंने फिर से गला फाड़ कर. चीख कर कहा!
नहीं! कोई शब्द नहीं सुनाई पड़ा! मेरा तो अजीज़, जबड़ा हिल, जबड़े की पेशियाँ हिलीं, जिव्हा हिली, गले ने, श्वास ऊपर छोड़ी, और बस! लेकिन? कोई शब्द ही नहीं निकले? ये कैसा मायाजाल? मायाजाल या फिर.... कोई त्रुटि? त्रुटि तो नहीं रह गई?
"माँ?" मैंने पुनः प्रयास किया!
"माँ?" पुनः एक बार फिर!
"रक्षाम! रक्षाम!" फिर से चीखा!
नहीं! कुछ नहीं! कोई शब्द न निकला मुख से! स्वर में, कोई कम्पन्न नहीं! मेरा बस, मुंह ही हिले, शब्द न निकलें! शब्द, कहाँ गए? क्या हुआ?
"माँ? रक्षाम!" पुनः विनती!
नहीं! फिर से वही सब! कोई स्वर नहीं! कोई भी स्वर नहीं!
"नहीं माँ! नहीं! नहीं! दया करो माँ! दया!" कहा मैंने,
अपने मूक शब्दों में! अब कोई मूक-भाषा समझे न समझे, माँ तो समझती ही है! उसी से गुहार लगाई मैंने! कई बार! कई कई बार!
"माँ? दर्शन दे माँ?" पुकारा मैंने,
बहुत देर तक....बहुत देर तक....जितना, खड़ा हो सकता था, हुआ, कांपते पांवों से, कांपती टांगों से, गुहार लगाता रहा! लगाता रहा! और जब, नहीं बन पड़ा, तो झुकता चला गया मैं! झुका, फिर से गुहार लगाई! अश्रु बह निकले! और फिर, झुकना भी असम्भव होने लगा, तो बैठ गया! बैठा, तो फिर से गुहार लगाने लगा! चीखने लगा! चीखता और फिर, हंसने भी लगा! कैसा मूर्ख हूँ मैं भी! कोई त्रुटि रही, तो भुगतना पड़ रहा है! हँसता, और हँसता! अपनी बेबसी पर हँसता! अपनी लाचारी पर हँसता! अपनी, विवशता पर हँसता! मेरे कारण, वो मासूम, वो अबोध, मेरी साधिका, उसका भी हन्ता बना गया मैं! हंसा! और हंसा! तेज! बहुत तेज! अफसोस! मेरे स्वर, मैंने ही न सुने तो दूजा कौन सुनता! ये सोच, फिर से हंसा! और हँसते हँसते, गिर पड़ा नीचे! अचेत होने तक, मेरे मुंह से, बस, हंसी ही उठती रही, स्वरहीन हंसी! और.....अचेतावस्था में जा गिरा मैं!
कितनी देर, कितना समय...न पता चला!
अचानक!
अचानक से मेरे नेत्र खुले! ये क्या? प्रकाश? स्वर्णिम-प्रकाश? कहाँ से? उठ बैठा! आसपास देखा! दूर दूर तक, बस, वही प्रकाश! बस वही! और कुछ नहीं! प्रकाश, अचानक से कौंध पड़ा! और जब कौंधा, तो ऊपर नेत्र गए! जो देखा! उसे देख..मैं खड़ा हो गया!
ऊपर, आकाश के स्थान पर, नीले से आभा वाले बादल से छाये थे! बिजली नहीं कड़क रही थी, लेकिन, आभास यही होता था! पश्चिमी क्षितिज से, केसरी प्रकाश उठने लगा था! चमकदार सा केसरी प्रकाश! मेरी जिव्हा, सिकुड़ सी गई थी! जबड़े, भिंच गए थे! नेत्र, चौड़े हो, उस अद्भुत, विहंगम से दृश्य को देखे जा रहे थे! तभी, फिर से प्रकाश कौंधा! लेकिन आँखें नहीं चुंधिया रही थीं! उत्तरी क्षितिज से, तेज लाल रंग का प्रकाश कौंधा, लाल, बादलों जैसा! तेजी से आगे आते हुए, केंद्र की ओर! मुझे लगा कि, पूर्वी क्षितज पर, जैसे कोई विस्फोट सा हुआ, लेकिन, कोई स्वर ही नहीं था! बस, गहरा नीला रंग, बिखरता चला गया! नीला रंग! गहरा नीला, ऐसा नीला गहरा रंग, मैंने कहीं नहीं देखा आज तक! उसके बादल भी जैसे, केंद्र की ओर, दौड़ पड़े थे! मैं, अपलक उस दृश्य को देख रहा था, लगता था, ब्रह्माण्ड की सृष्टि हो रही हो जैसे! फिर एक श्वेत प्रकाश! दक्षिणी क्षितिज से! श्वेत, चमकदार तारों के समूह का सा चंदीला रंग! उसमे, कई स्तम्भ से बने थे, वे भी, बादलों का रूप ले, दौड़े चले जा रहे थे केंद्र की ओर! कुछ ही क्षणों में वो मिश्रित हो गए! और फिर से, धीरे धीरे अन्धकार व्याप्त होने लगा! मैं खड़ा ही रहा! जब तक, पूर्ण अन्धकार न छा गया! यहां, सिम सी शान्ति थी! और न प्रकाश ही था, न कोई कण ही उसका शेष!
और तब! तब मेरे द्वारा बोले मंत्र, गूंज उठे! मेरे कानों में! एक एक करके! एक एक मंत्र! एक एक, जरठव! एक एक श्वास सी अंकीर्ण हो उनमे मेरी! दूर, चारों तरफ, दीये प्रज्ज्वलित हो गए! मेरे चारों ओर! एक के ऊपर एक! एक के ऊपर एक, दूर, आकाश तक, हर तरफ! अद्भुत! अद्भुत! बस! अद्भुत!
"माँ! मैं धन्य हुआ! धन्य!" कहा मैंने,
और अपने हाथ जोड़ लिए! खो गया मैं, माँ भैरवी की उपासना में! कितनी देर रहा? पता नहीं, स्वर गूंजे? पता नहीं! मैं वहीँ बैठता चला गया! तभी, प्रबल वायु वेग सा उठा! और मैं, उस में सवार होता सा, पीछे जा धकेला गया! कुछ देख नहीं पाया, कुछ सुन नहीं पाया! कुछ बोल भी न पाया! और जब रुका!
रुका तो नेत्र खुले!
ये? ये मैं कहाँ?
ओह! मस्तिष्क लौटा, संज्ञान हुआ!
"साधिके?" कहा मैंने, और, उठा मैं तब!
मैंने, देखा, उसको उठाया और लेता दिया नीचे! मेरी साधिका की देह, चांदी जैसे रंग से नहाई हुई थी! कोमलांगी सादृश थी वो! मैं उसको देख, मुस्कुरा पड़ा! बैठा उसके पास, उसके केश, संवारे, ठीक किये, उठा, और वस्त्र उढ़ा दिया उसकी देह को! और मैं भी, उस घाड़ को नमन कर, लेट गया संग अपनी साधिका के!
मित्रगण!
मेरी साधना पूर्ण हुई थी, और जो संगी आये थे, उनमे से एक की और हुई! मैं अपनी साधिका का आज तक ऋणी हूँ और सदैव ही रहूंगा!
साधिका के विषय में और कुछ नहीं लिखूंगा मैं, बस इतना..................कि उस साधना के बाद, मेरी साधिका, मृणा, फिर कभी किसी साधना में नहीं बैठी! कारण यही, कि वो, इस यात्रा, इसके अनुभव को, नहीं छोड़ सकती, नहीं भुला सकती!
ये संसार है! इस संसार में, सबकुछ यहीं है! बस, खोजने वाला होना चाहिए! खोजिए, और देखिये, क्या नहीं मिल जाता!
जय माँ उपाक्ष-भैरवी!
जय श्री भैरव नाथ!
साधुवाद!
aisi yatra ke baad sadhvi to sadhvi reh hi nahi gai hogi. Adbhut sansamaran. Jai shri Bhairav Nath Nirala.